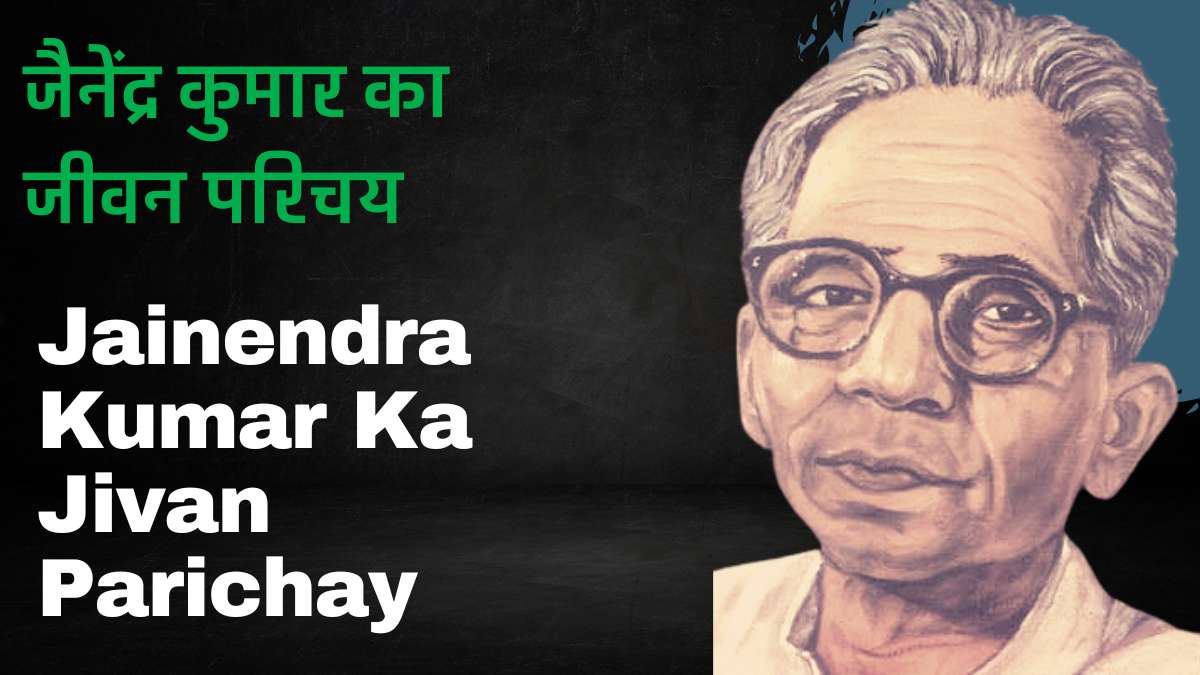| फ़ील्ड | जानकारी |
|---|---|
| नाम | जैनेंद्र कुमार |
| जन्म | 1905 |
| जन्मस्थान | अलीगढ़, उत्तर प्रदेश |
| रचनाएँ | परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्द्धन, मुक्तिबोध (उपन्यास); वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फाँसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब (कहानी-संग्रह); प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच-विचार, समय और हम (विचार-प्रधान निबंध-संग्रह) |
| पुरस्कार | साहित्य अकादेमी पुरस्कार, भारत-भारती सम्मान |
| मृत्यु | 1990 |
Contents
जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय :
जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी, 1905 को अलीगढ के कौड़ियागंज गाँव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। वह अपने उपन्यासों और कहानियों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं और एक साहित्यिक आलोचक के रूप में भी उनका सम्मान किया जाता है। उनके जन्म के दो साल बाद उनके पिता का निधन हो गया, और उनका पालन-पोषण उनकी माँ और मामा ने किया। उनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी, जहाँ जैनेन्द्र ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और दीक्षा ली। उनके परिवार का नाम आनंदीलाल था।
सन् 1912 में जैनेन्द्र गुरुकुल छोड़कर निजी तौर पर मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी के लिए बिजनौर चले गए। 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर के बजाय पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेंद्र ने अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राप्त की। 1921 में, उन्होंने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया और उस उद्देश्य के लिए दिल्ली आ गए। वे कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय के “राजनीति के तिलक स्कूल” में रहे, लेकिन अंततः उसे भी छोड़ दिया।
1921 से 1923 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यवसाय किया, जिसमें वे सफल भी हुए। हालाँकि, 1923 में वे नागपुर चले गए और राजनीतिक समाचार पत्रों में एक संवाददाता के रूप में काम करने लगे। उसी वर्ष उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने
को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है।
पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए किए वह
यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है?
जैनेंद्र कुमार की पुस्तकें और ग्रंथ:
| उपन्यास | कहानी संग्रह | निबंध संग्रह | अनूदित ग्रंथ | सह लेखन | संपादित ग्रंथ |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘परख’ (१९२९) | ‘फाँसी’ (१९२९) | ‘प्रस्तुत प्रश्न’ (१९३६) | ‘मंदालिनी’ (नाटक-१९३५) | ‘तपोभूमि’ (उपन्यास, ऋषभचरण जैन के साथ-१९३२) | ‘साहित्य चयन’ (निबंध संग्रह-१९५१) |
| ‘सुनीता’ (१९३५) | ‘वातायन’ (१९३०) | ‘जड़ की बात’ (१९४५) | ‘प्रेम में भगवान’ (कहानी संग्रह-१९३७) | ‘विचारवल्लरी’ (निबंध संग्रह-१९५२) | |
| ‘त्यागपत्र’ (१९३७) | ‘नीलम देश की राजकन्या’ (१९३३) | ‘पूर्वोदय’ (१९५१) | ‘पाप और प्रकाश’ (नाटक-१९५३) | ||
| ‘कल्याणी’ (१९३९) | ‘एक रात’ (१९३४) | ‘साहित्य का श्रेय और प्रेय’ (१९५३) | |||
| ‘विवर्त’ (१९५३) | ‘दो चिड़ियाँ’ (१९३५) | ‘मंथन’ (१९५३) | |||
| ‘सुखदा’ (१९५३) | ‘पाजेब’ (१९४२) | ‘सोच विचार’ (१९५३) | |||
| ‘व्यतीत’ (१९५३) | ‘जयसंधि’ ( |
जैनेंद्र कुमार: हिंदी के सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाकार:
हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा-धारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभूत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाज़ेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना-अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है।
कथाकार होने के साथ-साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक-सी दिखनेवाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन- दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन-जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है।
जैनेंद्र का “बाज़ार दर्शन” निबंध :
बाज़ार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्त्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाज़ारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले एक-डेढ़ दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाज़ार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है।
अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक-ठीक समझकर बाज़ार का उपयोग करें, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाज़ार में जाने के बजाय उसकी चमक-दमक में फँस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूलभाव को जैनेंद्र कुमार ने भाँति-भाँति से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज़ में, तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाज़ार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीतिशास्त्र बताया है।
जैनेंद्र कुमार: पुरस्कार / सम्मान:
- १९७१ में पद्म भूषण
- १९७९ में साहित्य अकादमी पुरस्कार